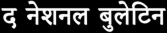मन्दिर यात्रा अब उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है जहाँ गम्भीर और पूर्वग्रहमुक्त पाठन की माँग है। कुछ शब्द, सामग्री और चित्रादि सम्वेदनशील जन को लज्जास्पद लग सकते हैं। हालाँकि गणित, स्थापत्य, ज्यामिति, साहित्यादि के कारण इसके रोचक होते जाने की भी आशंका है 😉 स्वविवेक से निर्णय लें कि इस चेतावनी के पश्चात आप पढ़ना चाहते/ती हैं या नहीं।
गिरिजेश जी आपके द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का डिजिटल जीर्णोद्धार बहुत अच्छा लगा. अभी कुछ समय पूर्व मैं भी भुवनेश्वर गया था. वहां से कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ पुरी और चंद्रभागा तट पर जाने का मौका भी मिला. मेरी दृष्टि आपकी तरह तीक्ष्ण, गहरी और व्यापक तो नहीं है पर फिर भी पुरी और आस पास के मंदिरों में दो चीजों ने मेरा ध्यान खीचा.पहला तो गज का शिकार करते हुए सिंह की एक विशेष प्रतिमा के दर्शन प्रत्येक मंदिर के द्वार पर हुए. इस मूर्ति में में गज को एकदम तुच्छ निरीह प्राणी के रूप में और सिंह को पुरी भव्यता के साथ दर्शाया गया है. सिंह देवी का वाहन है और जहाँ तक मैं समझता हूँ गज भगवान विष्णो को प्रिय है. भगवान जगन्नाथ की भूमि पर इस प्रकार के सिंह द्वार बनवाने का क्या कारण रहा होगा ये बात जानने की उत्सुकता मेरे मन में तभी से है. दूसरी बात जिसने मेरा ध्यान खीचा वो सम्भोग रत युगल की मूर्ति थी जो मुझे सभी मंदिरों में दिखाई दी. कोणार्क के सूर्य मंदिर में तो खुजराहो की ही तरह की मूर्तियों की भरमार है. मेरे साथ यात्रा कर रहे मेरे एक मेवाती सहयोगी ने बार बार मुझसे पूछा की भाई पंडित जी आपके मंदिरों में इस प्रकार की मूर्तियाँ क्यों होती है. मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया पर कभी ना कभी उसे जवाब देना जरुर चाहता हूँ. काश टाइम मशीन का अविष्कार हुआ होता.
जारी कोणार्क शृंखला की एक कड़ी में विचार शून्य ने मिथुन मूर्तियों से सम्बन्धित यह जिज्ञासा जताई थी:
… दूसरी बात जिसने मेरा ध्यान खीचा वो सम्भोग रत युगल की मूर्ति थी जो मुझे सभी मंदिरों में दिखाई दी. कोणार्क के सूर्य मंदिर में तो खुजराहो की ही तरह की मूर्तियों की भरमार है. मेरे साथ यात्रा कर रहे मेरे एक मेवाती सहयोगी ने बार बार मुझसे पूछा की भाई पंडित जी आपके मंदिरों में इस प्रकार की मूर्तियाँ क्यों होती है. मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया पर कभी ना कभी उसे जवाब देना जरुर चाहता हूँ. काश टाइम मशीन का अविष्कार हुआ होता.
खजुराहो और कोणार्क में कामक्रीड़ा एकदम नग्न रूप में बहुलता से चित्रित हुई है तो इतर प्राचीन मन्दिरों में भी इक्का दुक्का दबे ढके रूप में। प्रश्न यह उठता है कि देवालयों में इन्हें प्रदर्शित करते का क्या औचित्य? क्या तुक?
देवालय या आराधना के स्थल रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं के बाद आते हैं। शिक्षा इन तीनों के लिये पूर्वशर्त है – शिक्षा का अर्थ बस शालीय शिक्षा से न लें। मनुष्य अपने परिवेश से सम्मिलन, संयोग और विलयन के दौरान ही किसी परा शक्ति की सम्भावना पर सोचने लगता है।
लाखों वर्षों के विकास ने उसके मस्तिष्क में इतने प्रज्ञा मोड़ सृजित कर दिये हैं कि वह बिना सोचे रह ही नहीं सकता। पेट भरा हो, वस्त्र हों, सिर पर छत हो तो आगे क्या? इनसे आगे आता है परिष्करण और विचारों के प्रथम पग पर ही यह प्रश्न आ खड़ा होता है – सृष्टि कैसे? सृष्टि का होना, इसका नैरंतर्य, जन्म, जीवन और मृत्यु की एक विधि व्यवस्था का दिखना और परा शक्ति के आभास उसे स्वयं भी कुछ अद्भुत सृजित करने के लिये तैयार करते हैं लेकिन वह सृजन कैसा हो? उसका आधार क्या हो? पुन: उसे सृष्टि दिखती है और उसके साथ ही दिखते हैं परस्पर विरोधी से दिखते पूरक तत्त्व और उनका अद्भुत आपसी रमण – दिन-रात, प्रकाश-अन्धकार, मौन-ध्वनि और इनके साथ ही सामने आते हैं सर्वसत्य युग्म : स्त्री-पुरुष जिनके संयोग से सृष्टि का उद्भव होता है, जिनके संयोग के कारण ही नैरंतर्य है और जिनमें क्रीड़ा की वही वृत्ति है जो अन्य भौतिक युग्मों में दिखती है – विपर्यय और उसे बनाये रखते हुये योग, कुछ इस तरह कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्त्व ही न रहे। यह अद्भुत बाजीगरी ही परा शक्ति की परम अभिव्यक्ति लगती है।
स्त्री और पुरुष पदार्थ रूप में हैं लेकिन वातावरण के प्रभाव रूप भी वैसे ही हैं। यही प्रेक्षण अंतत: इस उद्घोष में अभिव्यक्त होता है – ईश्वर ने मनुष्य को निज रूप गढ़ा।
मनुष्य को लगता है कि वह उससे बिछड़ गया है और मृत्यु कुछ नहीं, उसके पास जाने का प्रस्थानबिन्दु भर है लेकिन मृत्यु होने तक वह उससे अलग क्यों रहे? परा शक्ति से जुड़ने और उसके आगे झुकने की चाह देवालयों का निर्माण करवाती है। ये निर्माता के अहंकार प्रतीक भी हो सकते हैं लेकिन मूल भाव वही रहते हैं और अभिमान की घोषणाओं में भी अनिवार्य रूप से अभिव्यक्त होते हैं।
तो अब जब मनुष्य को ईश्वर, उस परा शक्ति को गढ़ना है या उसके आगे झुकना है तो उसका रूप क्या हो? रूप को लेकर अनंत मान्यतायें और मार्ग हो सकते हैं लेकिन एक मार्ग सृजन के रूप से जुड़ता है – गर्भ में पलता पिंड धीरे धीरे बढ़ता है, निर्जीव से सजीव होता है और एक दिन जन्म भी लेता है। दिव्यता की ओर मनुष्य की यात्रा भी तो ऐसे ही होती है। यहीं मनुष्य का वह रूप सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय हो जाता है जो जन्म के पहले और बाद में भी पोसता है – माँ।
आश्चर्य नहीं कि प्रथम उपासना प्रकृति के रूप में कल्पित आदिम माँ की हुई। सरस्वती सभ्यता (सीमित ज्ञान के कारण पहले इसे सिन्धु नदी घाटी में सीमित कर दिया जाता था) में मातृपूजा के चिह्न अनायास ही नहीं हैं। बहुधा विश्लेषण करते हम भूल जाते हैं कि पूर्वजों ने आराधना को समग्रता में लिया। माँ होने के पहले सम्भोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्राचीन सभ्यताओं में संभोग गोपनीय कृत्य तो था लेकिन आजकल 😉 की तरह अपवित्र और लज्जास्पद कर्म नहीं था। इसलिये योनि और लिंग की पूजा मिलती है और ब्रह्मांडीय सम्भोग मिलन के मिथकीय चित्रण भी।
सरस्वती सभ्यता में मातृदेवी के साथ साथ ही विराट पुरुष भी है जिसे पशुपति कहा जाता है। वस्तुत: वह पुरुष देव है। उत्थित लिंग प्रमाण है। यहीं मुद्राओं में सम्भोग की कथित मिशनरी मुद्रा अंकित मिलती है जिसमें विराट पुरुष को लेटी हुई मातृदेवी के ऊपर झुके हुये दर्शाया गया है।